नारियल का पेड़, Cocos nucifera
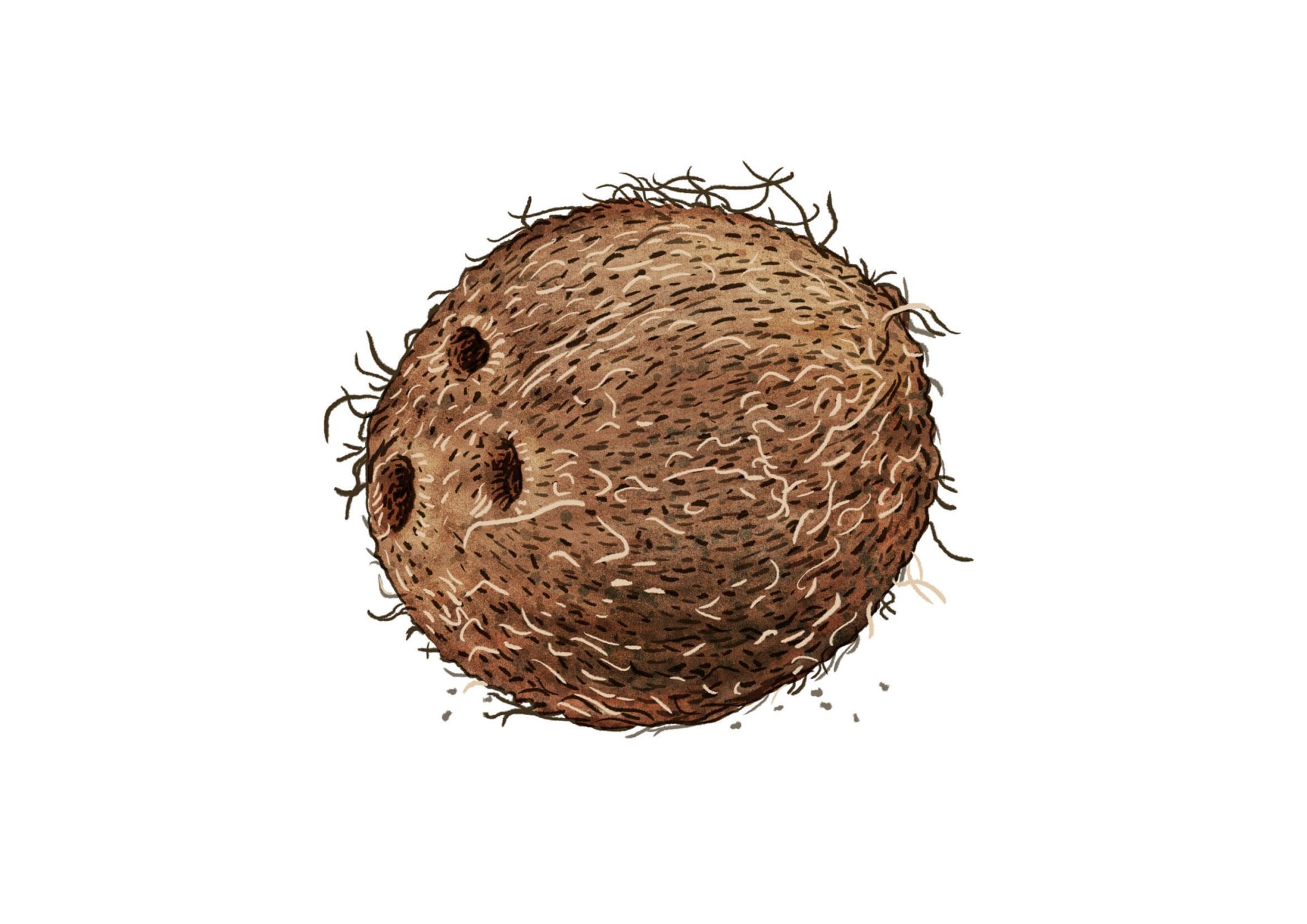
वैश्विक क्षेत्रफल: 11.1 मिलियन हेक्टेयर – और कुछ अवैध रूप से उपयोग की गई ज़मीनें
वेल्टेकर पर क्षेत्रफल: 14 वर्गमीटर (0.7%)
उत्पत्ति क्षेत्र: संभवतः मेलानीशिया (ऑस्ट्रेलिया के पास प्रशांत द्वीप समूह)
मुख्य उत्पादन क्षेत्र: इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत
उपयोग / मुख्य लाभ: खाद्य सामग्री, नारियल का तेल (कोकोनट फैट)
नारियल का पेड़ कई संस्कृतियों में आस्था और विश्वास का एक केंद्रीय प्रतीक है। नारियल को अक्सर उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण-पूर्व एशिया, ओशिनिया और पूर्वी अफ्रीका के कई क्षेत्रों में नारियल के पेड़ को “जीवन का वृक्ष” माना जाता है, और इसे मानव का प्रतिबिंब (अल्टर ईगो) भी कहा जाता है – यानी एक ऐसा पौधा जो मानव के भाग्य से गहरे रूप से जुड़ा है। कुछ समुदायों में माता-पिता अपने नवजात बच्चे को एक नारियल का अंकुर उपहार में देते हैं, जिसे वे बच्चे की नाल के साथ ज़मीन में लगाते हैं।
एक भारतीय कहावत कहती है: “नारियल के पेड़ के 999 उपयोग हैं, और 1000वाँ अभी तक खोजा नहीं गया है।” वास्तव में, इस पेड़ के सभी हिस्सों – जड़ से लेकर शीर्ष तक – किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं।
साल में चालीस फल तक
नारियल का पेड़ एक एकल-गृह पौधा होता है, यानी इसमें नर और मादा फूल एक ही पेड़ पर होते हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसार, नारियल असली नट नहीं होता, बल्कि यह एक कठोर बीज वाला फल होता है – जैसे चेरी या आलूबुखारा। इसका रेशेदार आवरण चमड़े जैसी बाहरी फल की दीवार से घिरा होता है और यही गूदा कहलाता है। इसके अंदर की पतली बीज-छिलक, उसमें मौजूद सख्त बीज-गूदा और नारियल पानी व अंकुर – ये सब मिलकर बीज का केंद्र बनाते हैं। एक लगभग 30 मीटर ऊँचे नारियल के पेड़ की ऊपरी छतरी में एक साल के भीतर सिर के आकार के करीब 40 फल तक पक सकते हैं। चयन और संकरण (क्रॉस ब्रीडिंग) के ज़रिए ऐसी कई किस्में विकसित की गई हैं जो विशेष रूप से अधिक उत्पादन देने वाली, बीमारियों से लड़ने वाली और उष्णकटिबंधीय तूफानों के प्रति सहनशील होती हैं।
नारियल का पेड़ भूमध्य रेखा के पास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी उत्तर और दक्षिण कर्क रेखा के बीच, समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊँचाई तक सबसे अच्छी तरह उगता है। हालाँकि, जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, फल देने की मात्रा कम होती जाती है। इस पेड़ को सालभर गर्म तापमान और नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन मिट्टी की उर्वरता को लेकर यह ज़्यादा मांग नहीं करता। एक नारियल का पेड़, उसकी उम्र, स्थान और देखभाल के अनुसार, हर साल लगभग 30 से 150 नारियल दे सकता है। इससे लगभग 10 से 20 किलो कोपरा (सूखा हुआ नारियल गूदा) प्राप्त होता है, जिससे या तो नारियल का तेल निकाला जाता है या कसा हुआ नारियल (नारियल बुरादा) बनाया जाता है।
नारियल का इतिहास
उत्तर-पश्चिम भारत के रेगिस्तान में मिली एक जीवाश्म नारियल से यह अनुमान लगाया गया कि नारियल की उत्पत्ति पश्चिमी गोंडवाना लैंड से हुई थी – एक प्राचीन महाद्वीप, जिसमें आज का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका शामिल थे। जब यह महाद्वीप लगभग 200 से 130 मिलियन वर्ष पहले टूटना शुरू हुआ, तो नारियल की प्रजातियाँ उस समय बन रहे टेथिस सागर के किनारों पर विकसित होने लगीं। नारियल के बीज महीनों तक अंकुरित होने योग्य बने रहते थे और वे समुद्र में तैरते हुए दूर-दराज़ के तटों तक पहुँचकर फैलते चले गए।
नारियल हज़ार साल से भी पहले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु के रूप में उपयोग में लिया जाने लगा था। हमें पता है कि सन् 912 में, सुंडा द्वीपों से नारियल मेसोपोटामिया के खलीफा के दरबार तक पहुँचाए गए थे। मध्य युग में तीर्थयात्री और अरब व्यापारी इस फल को यूरोप तक लेकर आए। 16वीं सदी के अंत में पुर्तगाली उपनिवेशवादी नाविकों ने ऐसे नारियल के प्याले, जिन्हें सोने या चांदी में जड़ा गया था, राजघरानों और पादरियों के पास पहुँचाया। यूरोप के लिए नारियल के पेड़ के आर्थिक महत्व को सबसे पहले स्पेनियों ने पहचाना, जिन्होंने 18वीं सदी के मध्य में फिलीपींस में इसकी खेती शुरू करवाई। लगभग 100 साल बाद, डचों ने श्रीलंका (तब का सीलोन) में इसका अनुसरण किया। शुरुआत में नारियल की खेती नारियल के रेशों से जहाज़ों की रस्सियाँ बनाने के लिए होती थी। बाद में, नारियल के तेल का उपयोग साबुन और मोमबत्तियाँ बनाने में होने लगा। 19वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी रसायनशास्त्रियों ने नारियल तेल का इस्तेमाल करके मार्जरीन (मक्खन का पौध आधारित विकल्प) बनाने में सफलता पाई।
इसके बाद, उत्पादक देशों में नारियल की खेती का क्षेत्रफल और नारियल तेल व कोपरा का निर्यात लगातार बढ़ता चला गया।
आज नारियल का पेड़, जो तेल का स्रोत है, साफ़-सफ़ाई और खाद्य उद्योग में उपयोग के लिए तेल ताड़, सूरजमुखी, सरसों और सोयाबीन जैसी अन्य फसलों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। अब कई उत्पादक देश यह प्रयास कर रहे हैं कि वे नारियल आधारित तैयार और अर्ध-तैयार उत्पादों का उत्पादन अपने देश में ही करें, साथ ही, पुराने पेड़ों की लकड़ी, नारियल पानी, और कठोर छिलकों जैसे उप-उत्पादों को भी नई-नई चीजों में इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए भी काम हो रहा है।
1961 से 2014 के बीच, FAO के अनुसार, नारियल की खेती का क्षेत्रफल 5.2 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर हो गया – यानी यह दोगुना से भी ज़्यादा हो गया। इसके बाद से खेती का क्षेत्रफल या तो स्थिर रहा है या थोड़ा घटा है – लेकिन उत्पादन क्षमता बढ़ी है। 2022 में पूरी दुनिया में लगभग 62.5 मिलियन टन नारियल की कटाई हुई। इसमें से तीन-चौथाई हिस्से का उत्पादन तीन सबसे बड़े उत्पादक देशों – इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत – से आया। अन्य देश जैसे श्रीलंका, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी और थाईलैंड इस सूची में बहुत पीछे हैं। हालाँकि, वास्तविक वैश्विक खेती का क्षेत्रफल इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई छोटे किसान नारियल की खेती मिश्रित प्रणालियों (जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री) में करते हैं, और उनकी फसलें स्थानीय रूप से उपयोग में ली जाती हैं, जिससे वे औपचारिक व्यापार आँकड़ों में शामिल नहीं होतीं। नारियल तेल के सबसे बड़े आयातक हैं: यूरोपीय संघ के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मलेशिया।
फल, तेल, औज़ार, दवा – नारियल का बहुपयोग
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नारियल का तेल पारंपरिक रूप से खासकर तलने और भूनने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ स्थानों पर पकी हुई नारियल की गिरी इतनी मीठी होती है कि इसे खाने में मिठास के लिए उपयोग किया जा सकता है, जबकि अन्य जगहों पर यह थोड़ी नमकीन स्वाद वाली भी हो सकती है। लगभग आठ महीने पुराने नारियल का पानी आज भी एक लोकप्रिय ताज़ा पेय माना जाता है। नारियल पानी में चीनी मिलाकर उसे अलग-अलग तरीकों से शराब या नारियल सिरके में बदला जा सकता है। फिलीपींस, भारत और श्रीलंका में एक खास मिठाई है – “नाटा डे कोको”, जो जेली जैसी होती है और जिसे या तो कैंडीड रूप में सीधे खाया जाता है, या डेसर्ट और डिब्बाबंद पेय के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि इन देशों में नारियल का तेल ताड़ के तेल से ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए वहाँ ताड़ के तेल का उपयोग बढ़ रहा है, जबकि अधिक से अधिक नारियल तेल विदेशों में, जहाँ क्रय शक्ति अधिक है, निर्यात किया जा रहा है।
नारियल का कठोर खोल, अपनी प्राकृतिक आकार के कारण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक आदर्श घरेलू बर्तन रहा है – जिसका उपयोग खाने-पीने, तेल रखने और कई अन्य चीज़ों के लिए किया जाता था और आज भी किया जाता है। इस मजबूत खोल से चम्मच, चाकू, छन्नी जैसे घरेलू औज़ार बनाए जाते हैं। खाली नारियल के खोल को प्राकृतिक ध्वनि गूंजने वाले पात्र के रूप में भी इस्तेमाल किया गया – जैसे कि रासल, बांसुरी जैसे संगीत वाद्ययंत्रों में। नारियल के खोल से कमरबंद, हार और अन्य गहने भी बनाए जाते रहे हैं। परंपरागत चिकित्सा में भी नारियल का प्रयोग होता रहा है – जैसे कि उसकी राख को त्वचा रोग, गठिया, सिरदर्द और पेट दर्द के इलाज में उपयोग किया गया। 1950 के दशक में, वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हुआ कि नारियल पानी स्वच्छ (स्टेराइल) होता है।
इसके बाद इसे पश्चिमी चिकित्सा में भी अपनाया गया – जैसे कि इंफ्यूज़न (ड्रिप) देने के लिए या लंबे समय तक दस्त होने पर निर्जलीकरण से बचाने के लिए।
नारियल का कठोर खोल एक बेहतरीन ईंधन सामग्री है, जो तेज़ गर्मी देता है लेकिन बहुत कम धुआँ बनाता है। इससे बनाई गई लकड़ी की कोयला (चारकोल) को पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाउडर के रूप में दाँत साफ़ करने के लिए और रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पश्चिमी देशों में इसे बार्बेक्यू कोयले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और एक्टिवेटेड चारकोल (सक्रिय कोयला) के रूप में यह रंग हटाने वाले और गंध दूर करने वाले उत्पादों में डाला जाता है। नारियल खोल का बारीक पाउडर आज कृत्रिम गोंदों और कई प्लास्टिक उत्पादों में भी मिलाया जाता है। हाल ही में भारत में, इस मजबूत पत्थर जैसे पदार्थ को कंक्रीट ईंटों में प्रयोगात्मक रूप से शामिल किया जा रहा है।
क्या नारियल तेल सच में सुपरफूड है?
हाल के वर्षों में विकास से जुड़ी सोच रखने वाले संगठन और कंपनियाँ यह प्रयास कर रही हैं कि नारियल तेल जैसे नवीकरणीय संसाधन का उत्पादन और व्यापार न्यायसंगत व्यापार (फेयर ट्रेड) और टिकाऊ, भविष्य-उन्मुख विकास के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसका उद्देश्य है कि उष्णकटिबंधीय देशों में नारियल उगाने वाले छोटे किसान परिवारों की जीवन स्थितियों में सुधार किया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनाया जा सके।
फिर भी – ताड़ के तेल की तरह ही, नारियल तेल में भी मुख्य रूप से संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, और नारियल तेल में इनकी मात्रा लगभग 90 प्रतिशत होती है। संतृप्त वसा अम्लों को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल (खराब कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाते हैं और इनका संबंध हृदय और रक्त संचार से जुड़ी बीमारियों के बढ़े हुए खतरे से जोड़ा जाता है। हालाँकि आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पर थोड़ा अधिक संतुलित हो गया है, फिर भी यह कहना कि नारियल कोई “सुपरफूड” है और विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक है, वैज्ञानिक आधार से पूरी तरह रहित है और यह सिर्फ विज्ञापन का दावा है।
असल में, कई देशों को नारियल तेल (या ताड़ के तेल) पर निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से ही स्थानीय स्तर पर पर्याप्त तेल देने वाले पौधे मौजूद हैं – जैसे कि यूरोप में जैतून, सरसों और सूरजमुखी। स्थानीय खेती का मतलब होता है कि
हमें वर्षावनों की कटाई, संदिग्ध खेती के तरीके, ज़मीन हथियाना और खराब मज़दूरी स्थितियों जैसी समस्याओं से बचना मिल सकता है – जो अक्सर उष्णकटिबंधीय तेल उत्पादक देशों में देखने को मिलती हैं। और सबसे ज़रूरी बात: स्थानीय उत्पादन से हम हज़ारों किलोमीटर लंबे वैश्विक परिवहन मार्गों की ज़रूरत भी कम कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है।
क्या नारियल के पेड़ ताड़ के पेड़ों से बेहतर हैं?
तेल ताड़ या नारियल ताड़ न तो स्वभाविक रूप से खराब होते हैं और न ही अत्यंत अच्छे। समस्या असल में दुनिया भर में वनस्पति तेलों और वसा की भारी माँग में छिपी है। उद्योगों को जिन विशाल मात्रा में तेल की ज़रूरत होती है, उसे सबसे सस्ते तरीके से औद्योगिक स्तर की एकल फसल वाली खेती में और अक्सर शोषणपूर्ण श्रम स्थितियों के तहत ही उगाया जा सकता है।
तेल ताड़ के मुकाबले, नारियल के पेड़ों की खेती में अब तक तेज़ और भारी विस्तार नहीं हुआ है। पिछले दस वर्षों में तो खेती का क्षेत्र लगभग स्थिर ही रहा है। सामान्य तौर पर, नारियल की खेती में इतनी बड़ी-बड़ी प्लांटेशन या अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ नहीं हैं,
जितनी कि ताड़ के तेल के मामले में देखी जाती हैं। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है, इसलिए इसे बहुपयोगी पौधा माना जाता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह इनका पूरा उपयोग भी किया जाता है। प्लांटेशन में बड़ी मात्रा में नारियल के अवशेष निकलते हैं, जो अक्सर ना तो उपयोग में लाए जाते हैं, और ना ही ठीक तरह से कम्पोस्ट किए जाते हैं।
स्रोत
Spektrum: Die Kokospalme – Baum der tausend Möglichkeiten. Link.
Rettet den Regenwald e.V.: Kokosöl – Keine gute Alternative zu Palmöl. Link.
WWF: Like Ice in the Sunshine: Pflanzenöle und Fette im Speiseeis. Das Beispiel Kokosöl. Link.





